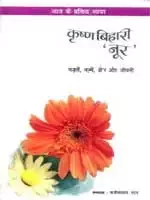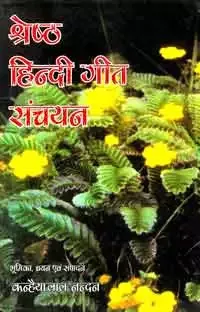|
गजलें और शायरी >> आज के प्रसिद्ध शायर - कृष्णबिहारी नूर आज के प्रसिद्ध शायर - कृष्णबिहारी नूरकन्हैयालाल नंदन
|
205 पाठक हैं |
||||||
भारत के उर्दू शायरों में कृष्णबिहारी नूर एक मशहूर नाम है। प्रस्तुत है उनकी चुनी हुई गजलें नज्में शेर और जीवन परिचय
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
भारत के उर्दू शायरों में कृष्णबिहारी नूर एक
मशहूर नाम है। एक तरफ उनकी
शायरी जहाँ सूफियाना अन्दाज में मस्त कलन्दरों की तरह अपना दाखिला दर्ज
कराती है वहाँ दूसरी तरफ हिन्दू दर्शन और अध्यात्म की खुशबुएँ बिखेरती है।
इक नूर की लकीर सी खिंचती चली गई
मैं उन दिनों दो-तीन बरसों के लिए फिर से
बम्बई रह रहा था। न्यूज़ के चैनल
में एक नई न्यूज़ स्टाइल की शुरुआत करनी थी। ‘इनटाइम’
न्यूज़ का ख़ाका तैयार करने वाले दिन थे। मैं प्रिंट मीडिया का एक आदमी एक
चुनौती लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दाखिल हो गया था। नूर साहब ने सुना
कि मैं बम्बई में रह रहा हूँ। (माफ़ कीजिए, मुम्बई कहना चाहिए, अब यही सही
नाम है।) सो एक दिन वासी से फ़ोन आया। वासी नई मुम्बई का इलाक़ा है जो
मुख्य मुम्बई से कम से कम एक-डेढ़ घण्टा दूर है। नूर साहब वहीं कहीं ठहरे
हुए थे और किसी मुशायरे के सिलसिले में मुम्बई गए हुए थे। मुशायरा एक दिन
बाद था। आवाज़ आई : ‘‘नन्दन जी, मैं नूर बोल रहा हूँ।
आपसे मिलना चाहूँ तो कैसे मिल सकता हूँ ?’’
ज़ाहिर है, नूर साहब का इस तरह मुहब्बत से फ़ोन करना मुझे अन्दर तक पिघला गया। बोले, मैं अभी आना चाहता हूँ। और साहब एक-डेढ़ घंटे बाद नूर साहब मेरे दफ़्तर हाज़िर !
सच कहूँ तो मुझे लगा कि नूर साहब को किसी ने मेरे चैनल पर किसी सीरियल के सिलसिले में पटाया है जिसकी सिफ़ारिश लेकर नूर साहब को इतनी दूर से आना पड़ा है। इसी ग़लतफ़हमी में मैंने नूर साहब से इतनी दूर आने का मक़सद जानने की पेशकश की। ‘‘कुछ नहीं, एक नई ग़जल हुई है। लगा कि आप कहीं मिल जाएँ तो सुनाऊँ,’’ नूर साहब ने कहा।
मैं मन ही मन अपनी ग़लतफ़हमी पर शर्मिन्दा और नूर साहब के इस अन्दाज़ से बेहद ख़ुश हुआ। अपने को ख़ुशकिस्मत बताकर नूर साहब का शुक्रिया अदा किया कि वे इतनी दूर चलकर मुझसे मिलने आए। जवाब सुनकर मैं थोड़ा और लजा गया। ‘‘क्या बात कर रहे हैं आप ! अरे, आप जैसा संवेदनशील श्रोता समन्दर पार भी हो तो उस तक जाने की कोशिश करता, यह तो छोटी सी चेंबूर क्रीक लाँघ कर आया हूँ। लीजिए, ग़ज़ल का मतला मुजाहिज़ा हो।
कहा है कि—
ज़ाहिर है, नूर साहब का इस तरह मुहब्बत से फ़ोन करना मुझे अन्दर तक पिघला गया। बोले, मैं अभी आना चाहता हूँ। और साहब एक-डेढ़ घंटे बाद नूर साहब मेरे दफ़्तर हाज़िर !
सच कहूँ तो मुझे लगा कि नूर साहब को किसी ने मेरे चैनल पर किसी सीरियल के सिलसिले में पटाया है जिसकी सिफ़ारिश लेकर नूर साहब को इतनी दूर से आना पड़ा है। इसी ग़लतफ़हमी में मैंने नूर साहब से इतनी दूर आने का मक़सद जानने की पेशकश की। ‘‘कुछ नहीं, एक नई ग़जल हुई है। लगा कि आप कहीं मिल जाएँ तो सुनाऊँ,’’ नूर साहब ने कहा।
मैं मन ही मन अपनी ग़लतफ़हमी पर शर्मिन्दा और नूर साहब के इस अन्दाज़ से बेहद ख़ुश हुआ। अपने को ख़ुशकिस्मत बताकर नूर साहब का शुक्रिया अदा किया कि वे इतनी दूर चलकर मुझसे मिलने आए। जवाब सुनकर मैं थोड़ा और लजा गया। ‘‘क्या बात कर रहे हैं आप ! अरे, आप जैसा संवेदनशील श्रोता समन्दर पार भी हो तो उस तक जाने की कोशिश करता, यह तो छोटी सी चेंबूर क्रीक लाँघ कर आया हूँ। लीजिए, ग़ज़ल का मतला मुजाहिज़ा हो।
कहा है कि—
आग है पानी है मिट्टी है हवा है मुझमें
और फिर मानना पड़ता है ख़ुदा है मुझमें
अब तो ले-दे के वही शख़्स बचा है मुझमें
मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझमें
जितने मौसम हैं वो सब जैसे कहीं मिल जाएँ
इन दिनों कैसे बताऊँ जो फ़ज़ा है मुझमें
आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन
आईना इसमें है ख़ामोश कि क्या है मुझमें
टोक देता है, क़दम जब भी गलत उठता है
ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझमें
अब तो बस जान ही देने की है बारी ए ‘नूर’ !
मैं कहाँ तक करूँ साबित कि वफ़ा है मुझमें।
और फिर मानना पड़ता है ख़ुदा है मुझमें
अब तो ले-दे के वही शख़्स बचा है मुझमें
मुझको मुझसे जो अलग करके छुपा है मुझमें
जितने मौसम हैं वो सब जैसे कहीं मिल जाएँ
इन दिनों कैसे बताऊँ जो फ़ज़ा है मुझमें
आईना ये तो बताता है मैं क्या हूँ लेकिन
आईना इसमें है ख़ामोश कि क्या है मुझमें
टोक देता है, क़दम जब भी गलत उठता है
ऐसा लगता है कोई मुझसे बड़ा है मुझमें
अब तो बस जान ही देने की है बारी ए ‘नूर’ !
मैं कहाँ तक करूँ साबित कि वफ़ा है मुझमें।
पाँचों तत्वों से बने इन्सान की कैफ़ियत पहले
ही शे’र में तुलसी
की अर्धाली ‘क्षिति जल पावक गगन समीरा’ के समानान्तर
जाकर खड़ी हो गई। शे’र मुकम्मल हुआ ‘अहं
ब्रह्मास्मि’ में। ये हैं जनाब कृष्ण बिहारी
‘नूर’ जो लखनऊ से चलकर मुम्बई पहुँचे थे और मेरे ऊपर
इतने मेहरबान थे कि अपनी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ करने वासी से अंधेरी
(मुम्बई का पश्चिमी उपनगर) आए थे। मेरे हाफ़िज़े में वह दिन और
‘नूर’ साहब की आवाज़ के उतार-चढ़ाव उनके जिस्म के
सारे हरकात के साथ महफ़ूज हैं। उनकी शायरी की अदायगी उनके अशआर की तहें
खोलती चलती है। तहत में पढ़ते हैं लेकिन शेरख़्वानी का उनका यह
तहतुल-लफ़्ज़ अन्दाज़ अपने आप में एक ऐसी कला है जो तरन्नुम की मोहताजी से
कोसों दूर है। नूर साहब को इस कला का ऐसा प्रसाद मिला हुआ है कि उनसे यह
सीखा जा सकता है कि शे’र पढ़ने का सही तरीक़ा क्या होता है।
उर्दू के मशहूर समीक्षक जनाब ज़ोए अंसारी ने बम्बई के ही एक दैनिक अख़बार
‘इन्क़लाब’ में पन्द्रह साल पहले लिखा था कि इसके लिए
‘‘न तरन्नुम की मुहताजी थी, न ख़ुशगुलू या ख़ुशरू
होने की ज़रूरत। स्टेज से शे’र को यूँ अदा करना कि मफ़हूम (आशय)
तस्वीर बनकर आँखों में फिर जाए। बुज़ुर्गों का यह वरसा (उत्तराधिकारी)
‘नूर’ लखनवी को मिला और इतना मिला है कि उनकी नज़ीर
कहीं नज़र नहीं आती।’’
यह मेरी ख़ुशकिस्मती है कि उनके साथ मैंने दर्जनों बार मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शिरकत की है और उनके शे’र पढ़ने के हुनर का जलवा हाज़रीन के चेहरों पर छपा हुआ देखा है। इस जलवे का जलाल तब भी मद्धम नहीं पड़ा जब डॉक्टरों ने उनके बाईपास के बाद उन्हें थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी। अभी बाईपास के सारे असरात से फ़ारिग नहीं हुए थे कि लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो ने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जिसमें हिन्दी-उर्दू दोनों की नुमाइंदगी थी। बाईपास के पास पहला मुशायरा पढ़ने आए थे इसमें ‘नूर’ साहब। दिल्ली से मैं भी शरीक़े-महफ़िल था सो चश्मदीद वाक़या बयान कर रहा हूँ कि जब ‘नूर’ साहब को पढ़ने की दावत दी गई तो रेडियो ने उन्हें सहूलियत से काम-अंजाम देने के लिए जहाँ बैठे थे, वहीं से पढ़ने की सुविधा देनी चाही। ‘नूर’ साहब ने अपना बाईपास रखा किनारे और हाज़रीन से मुख़ातिब होते हुए बोले : ‘‘आप माफ़ी दें, डॉक्टरों ने दिल चीर कर रख दिया लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरा दिल मेरे पास है, ही नहीं; वह तो मेरे चाहने वाले आप जैसे लोगों के पास है, सो शेर मुलाहज़ा हो...’’ और फिर तो साहब ‘नूर’ साहब ने ऐसे पढ़ा जैसे पिंजरे से निकल के परिन्दे ने बेख़ौफ़ उड़ानें भरी हों। ग़ज़ल भी वो पढ़ी जो उनकी ग़ज़लों में मेरी सबसे पसन्दीदा ग़ज़ल है। बल्कि उसका एक शे’र तो मेरे जीवन दर्शन का एक हिस्सा बन चुका है :
यह मेरी ख़ुशकिस्मती है कि उनके साथ मैंने दर्जनों बार मुशायरों और कवि सम्मेलनों में शिरकत की है और उनके शे’र पढ़ने के हुनर का जलवा हाज़रीन के चेहरों पर छपा हुआ देखा है। इस जलवे का जलाल तब भी मद्धम नहीं पड़ा जब डॉक्टरों ने उनके बाईपास के बाद उन्हें थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी। अभी बाईपास के सारे असरात से फ़ारिग नहीं हुए थे कि लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो ने एक कवि सम्मेलन आयोजित किया जिसमें हिन्दी-उर्दू दोनों की नुमाइंदगी थी। बाईपास के पास पहला मुशायरा पढ़ने आए थे इसमें ‘नूर’ साहब। दिल्ली से मैं भी शरीक़े-महफ़िल था सो चश्मदीद वाक़या बयान कर रहा हूँ कि जब ‘नूर’ साहब को पढ़ने की दावत दी गई तो रेडियो ने उन्हें सहूलियत से काम-अंजाम देने के लिए जहाँ बैठे थे, वहीं से पढ़ने की सुविधा देनी चाही। ‘नूर’ साहब ने अपना बाईपास रखा किनारे और हाज़रीन से मुख़ातिब होते हुए बोले : ‘‘आप माफ़ी दें, डॉक्टरों ने दिल चीर कर रख दिया लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरा दिल मेरे पास है, ही नहीं; वह तो मेरे चाहने वाले आप जैसे लोगों के पास है, सो शेर मुलाहज़ा हो...’’ और फिर तो साहब ‘नूर’ साहब ने ऐसे पढ़ा जैसे पिंजरे से निकल के परिन्दे ने बेख़ौफ़ उड़ानें भरी हों। ग़ज़ल भी वो पढ़ी जो उनकी ग़ज़लों में मेरी सबसे पसन्दीदा ग़ज़ल है। बल्कि उसका एक शे’र तो मेरे जीवन दर्शन का एक हिस्सा बन चुका है :
मैं एक क़तरा हूँ मेरा अलग वजूद तो है
हुआ करे जो समन्दर मेरी तलाश में है।
हुआ करे जो समन्दर मेरी तलाश में है।
इसमें मामूली इन्सान की मामूलियत भी अपने
अस्तित्व को स्वाभिमान के साथ
जीने का एहसास देती है। समन्दर की हस्ती बहुत बड़ी है, उसके सामने बूँद का
कोई स्थान नहीं लेकिन जब तक अलग है तब तक वह बूँद तो कही जाती है। समन्दर
में मिलने के बाद तो दरिया भी दरिया नहीं रह जाता। जगन्नाथ दास
‘रत्नाकर’ ने ‘उद्धव शतक’ में
गोपियों को निराकार ब्रह्म के मुकाबले बूँद के रूप में रखते हुए इस तर्क
से उद्धव को ठगा सा वापस भेज दिया था। गोपियों ने कहा था कि
‘‘उधो, हम तुम्हारे निराकार ब्रह्म में समा गईं तो
तुम्हारे ब्रह्म का तो भला क्या बने-बिगड़ेगा, लेकिन हमारा अस्तित्व खत्म
हो जाएगा, हम विलीन हो जाएँगी :
जइहै बनि बिगरि न बारिधिता बारिधि की
बूँदता बिलैहै बूँद बिबस बिचारी की।
बूँदता बिलैहै बूँद बिबस बिचारी की।
माना कि हम बूँद हैं लेकिन अभी ब्रह्म से अलग
हमारी बूँदता सुरक्षित है,
ब्रह्म में मिलते ही हमारी बूँदता ही बिला जाएगी, गायब हो जाएगी। उसी को
नूर साहब ने अपने ढंग से कहा कि ‘‘मैं एक क़तरा हूँ
मेरा अलग वजूद तो है। हुआ करे जो समन्दर मेरी तलाश में
है।’’
नूर साहब पुराने उस्तादों के ही नहीं, अपने कहे अशआर को भी और आगे बढ़ाने की कोशिशें करते रहते हैं। इसी ग़जल का एक शे’र है :
नूर साहब पुराने उस्तादों के ही नहीं, अपने कहे अशआर को भी और आगे बढ़ाने की कोशिशें करते रहते हैं। इसी ग़जल का एक शे’र है :
मैं जिसके हाथ में इक फूल दे आया था
उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है।
उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है।
एक जगह फ़िराक़ साहब ने भी कहा है कि
‘बेतअल्लुक़ न मुझसे हो ऐ
दोस्त बदसलूक़ी तेरी मुझे मंजूर।’’
नूर साहब ने अपने शे’र और फ़िराक़ साहब के शे’र, दोनों को आगे ले जाने की पेशकश की। फ़रमाते हैं :
नूर साहब ने अपने शे’र और फ़िराक़ साहब के शे’र, दोनों को आगे ले जाने की पेशकश की। फ़रमाते हैं :
बेतअल्लुक़ी उसकी कितनी जानलेवा है
आज हाथ में उसके फूल है न पत्थर है।
आज हाथ में उसके फूल है न पत्थर है।
श्याम गौर किमि कहऊँ बखानी
गिरा अनयन, नयन बिनु बानी
गिरा अनयन, नयन बिनु बानी
आँखों ने वह स्वरूप देखा है लेकिन उनके पास
वाणी नहीं है और वाणी बखान कर
सकती है लेकिन उसने वह रूप देखा नहीं। इसे असग़र गोंडवी ने भी यों भी बयान
किया है :
तेरे जलवों के आगे हिम्मते शरहो बयाँ रख दी
ज़ुबाने बे-निगह रख दी निगाहे-बेज़ुबाँ रख दी।
ज़ुबाने बे-निगह रख दी निगाहे-बेज़ुबाँ रख दी।
नूर साहब ने भी इस पर अपनी ज़ेहन-आज़माइश की
और कहा :
हो किस तरह से बयाँ तेरे हुस्न का आलम
ज़ुबाँ नज़र तो नहीं है नज़र ज़ुबाँ तो नहीं।
ज़ुबाँ नज़र तो नहीं है नज़र ज़ुबाँ तो नहीं।
फ़िराक़ साहब का एक शे’र लेकर इसका
एक और उदाहरण सामने रखना
चाहूँगा। फ़िराक़ साहब का बड़ा मशहूर शे’र है :
तुम मुख़ातिब भी हो क़रीब भी हो
तुमको देखूँ कि तुमसे बात करूँ
तुमको देखूँ कि तुमसे बात करूँ
नूर साहब इस शे’र को अपने ढंग से
कहने को यों मजबूर हुए :
किस तरह मैं देखूँ भी बातें भी करूँ तुमसे
आँख अपना मज़ा चाहे दिल अपना मज़ा चाहे।
आँख अपना मज़ा चाहे दिल अपना मज़ा चाहे।
इस तरह ‘नूर’ लखनवी
दूसरों के खूबसूरत अशआर से
मुतास्सिर होकर उन पर अपने रंग की मोहर लगाने के हुनर और फ़न के उस्ताद
शायर हैं। दूसरों के ही नहीं, अपने अशआर पर भी नई-नई रंगतें जड़ने का काम
वे करते रहते हैं लेकिन दूसरे के शे’र को अपने नाम पर जड़ लेने
का हुनर उन्हें नहीं आया। एक बार ऐसी चूक, अंजुम रूमानी के एक
शे’र को बहुत पहले सुनने के बाद भूल जाने पर, उनसे हो चुकी है
कि जिसका प्रायश्चित्त उन्होंने इस वाक़ये को सार्वजनिक रूप से लिखकर किया
है। अब उनकी वह ग़ज़ल बेहद मशहूर ग़ज़लों में से है :
तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था
कोई न जान सका रखरखाव ऐसा था।
कोई न जान सका रखरखाव ऐसा था।
मशहूर ग़ज़लों का जिक्र करूँ तो तमाम ग़ज़लें
हैं जो चाहने वालों की ज़बान
पर हैं। तमाम ग़ज़लें मशहूर गायकों ने गायी हैं जिनके रिकार्ड उपलब्ध हैं।
‘रुक गया आँख से बहता हुआ दरिया कैसे’ तो कई-कई
गायकों ने गाया है। इसे असलम खान का भी स्वर मिला है, गुलाम अली का भी।
भूपेन्द्र, छाया गाँगुली, पीनाज़ मसानी, रवीन्द्र जैन, राजकुमार रिज़्वी,
शीला महेन्द्रू, अहमद हुसैन-मुहम्मद हुसैन जैसे गायकों ने भी उनकी कुछ
चुनिंदा ग़ज़लों को अपने स्वर दिए हैं।
कुछ अशआर जो अक्सर लोगों के मुँह से सुने जाते हैं, यहाँ दे देना भी ग़ैर मुनासिब नहीं होगा। इन चन्द अशआर से ही नूर के कलाम की अज़मत (महत्ता) को आँका जा सकता है :
कुछ अशआर जो अक्सर लोगों के मुँह से सुने जाते हैं, यहाँ दे देना भी ग़ैर मुनासिब नहीं होगा। इन चन्द अशआर से ही नूर के कलाम की अज़मत (महत्ता) को आँका जा सकता है :
गुज़रे जिधर जिधर से वो पलटे हुए नक़ाब
इक नूर की लकीर-सी खिंचती चली गई।
देखा जो उन्हें सर भी झुकाना न रहा याद
दरअसल नमाज़ आज अदा हमसे हुई है
जहाँ मैं क़ैद से छूटूँ कहीं पे मिल जाना,
अभी न मिलना, अभी ज़िन्दगी की क़ैद में हूँ
लब क्या बताएँ कितनी अज़ीम उसकी ज़ात है
सागर को सीपियों से उलटने की बात है
मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था
घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था
मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई
हर शाम कोई आया, उठा ले गया मुझे
तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख
चेहरे पर तेरे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा
शख़्स मामूली वो लगता था मगर ऐसा न था
सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था
इतना बहुत है तुमसे निगाहें मिली रहें
अब बस करो शराब न दो, मैं नशे में हूँ
ये किस मुक़ाम पे ले आई जुस्तजू तेरी
कोई चिराग़ नहीं और रोशनी है बहुत
इक नूर की लकीर-सी खिंचती चली गई।
देखा जो उन्हें सर भी झुकाना न रहा याद
दरअसल नमाज़ आज अदा हमसे हुई है
जहाँ मैं क़ैद से छूटूँ कहीं पे मिल जाना,
अभी न मिलना, अभी ज़िन्दगी की क़ैद में हूँ
लब क्या बताएँ कितनी अज़ीम उसकी ज़ात है
सागर को सीपियों से उलटने की बात है
मैं तो अपने कमरे में तेरे ध्यान में गुम था
घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था
मुद्दत से एक रात भी अपनी नहीं हुई
हर शाम कोई आया, उठा ले गया मुझे
तुझसे अगर बिछड़ भी गया मैं तो याद रख
चेहरे पर तेरे अपनी नज़र छोड़ जाऊँगा
शख़्स मामूली वो लगता था मगर ऐसा न था
सारी दुनिया जेब में थी, हाथ में पैसा न था
इतना बहुत है तुमसे निगाहें मिली रहें
अब बस करो शराब न दो, मैं नशे में हूँ
ये किस मुक़ाम पे ले आई जुस्तजू तेरी
कोई चिराग़ नहीं और रोशनी है बहुत
मजाज़ी मसला है कि हक़ीक़ी, इसके बीच उनके
यहाँ बड़ा झीना पर्दा है।
साँसों के संगीत से वे आत्मा का गीत निकालते हैं सितार के पदों की तरह।
कृष्ण बिहारी ‘नूर’ की शायरी श्रृंगार से इसी तरह अध्यात्म तक आवाजाही करती है। वे मेहबूब की तस्वीर में कब परमपिता की तस्वीर चस्पाँ कर देते हैं, पता नहीं चलता। मेहबूब का चेहरा अर्थ के समन्दर में डुबोते ही आध्यात्मिक चिन्तन का चेहरा बन जाता है। मुरादाबाद के मंसूर उस्मानी का कहना है कि ‘‘नूर की शायरी मेहबूब के परदे में कहीं ख़ुद को और कहीं ख़ुदा को तलाश करने की वह साधना है जो शब्दों से तस्वीर बनाती है तो मेहबूब का चेहरा बन जाता है और अर्थ में डूबती है तो अध्यात्म का मंज़र बिखेर देती है। उनके शब्दों में कहूँ तो ‘नूर’ साहब ने अपने रचनात्मक चिन्तन के उद्यान में ग़म का बिस्तर बिछाया है, इश्क़ की चादर ओढ़ी है और ख़्वाबों का वो तकिया लगाया है जिसने उन्हें न तो ख़ुद से दूर किया, न ख़ुदा से। अपने इस शिकनों भरे बिस्तर पर ‘नूर’ साहब को अपने व्यक्तित्व की उस सच्चाई का एहसास हो गया है जहाँ ख़ुदी और ख़ुदा का फ़र्क़ भी स्पष्ट हो जाता है।’’
और इस फ़र्क़ को नूर साहब ने स्पष्ट भी कर दिया है :
कृष्ण बिहारी ‘नूर’ की शायरी श्रृंगार से इसी तरह अध्यात्म तक आवाजाही करती है। वे मेहबूब की तस्वीर में कब परमपिता की तस्वीर चस्पाँ कर देते हैं, पता नहीं चलता। मेहबूब का चेहरा अर्थ के समन्दर में डुबोते ही आध्यात्मिक चिन्तन का चेहरा बन जाता है। मुरादाबाद के मंसूर उस्मानी का कहना है कि ‘‘नूर की शायरी मेहबूब के परदे में कहीं ख़ुद को और कहीं ख़ुदा को तलाश करने की वह साधना है जो शब्दों से तस्वीर बनाती है तो मेहबूब का चेहरा बन जाता है और अर्थ में डूबती है तो अध्यात्म का मंज़र बिखेर देती है। उनके शब्दों में कहूँ तो ‘नूर’ साहब ने अपने रचनात्मक चिन्तन के उद्यान में ग़म का बिस्तर बिछाया है, इश्क़ की चादर ओढ़ी है और ख़्वाबों का वो तकिया लगाया है जिसने उन्हें न तो ख़ुद से दूर किया, न ख़ुदा से। अपने इस शिकनों भरे बिस्तर पर ‘नूर’ साहब को अपने व्यक्तित्व की उस सच्चाई का एहसास हो गया है जहाँ ख़ुदी और ख़ुदा का फ़र्क़ भी स्पष्ट हो जाता है।’’
और इस फ़र्क़ को नूर साहब ने स्पष्ट भी कर दिया है :
मैं जिस हुनर से हूँ पोशीदा अपनी ग़ज़लों
में
उसी तरह वो छुपा सारी कायनात में है।
उसी तरह वो छुपा सारी कायनात में है।
कुछ इसी तरह के हुनर से
‘नूर’ साहब अपने ज़ाती (निजी)
ग़म को कायनात का ग़म बना देते हैं। दोनों में कोई ऐसी लकीर नहीं है जिसके
ज़रिए देखा जा सके कि यहाँ उनका ज़ाती ग़म था, और यह कायनात का ग़म है।
चिन्तन की यह रचनात्मक बारीक़ी उनके स्वभाव में है। इसी स्वभाव ने उन्हें
सांसारिक सुखों से समझौता नहीं करने दिया, सूफ़ियों के ज्ञान मार्ग का
रास्ता सुझाया। उस रास्ते पर चलना तलवों को लहूलुहान करना है लेकिन उनका
हर लफ़्ज उसी रास्ते पर चलने को बेताब मिलता है। एक स्थायी नशा तारी है,
तार मिला हुआ है। इसी का नतीजा है कि वे वक्ती सियासत की बात भी करते हैं
तो लगता है दुनिया के सबसे बड़े हुक्मराँ की बात कर रहे हैं जिसके हाथ में
हम सबकी बागडोर है :
ग़रज़ कि नसीब में लिखी रही असीरी ही
किसी की क़ैद से छूटा किसी की क़ैद में हूँ।
किसी की क़ैद से छूटा किसी की क़ैद में हूँ।
इसी ग़ज़ल के कुछ और शे’र देखें,
लगता है इस जहाँ से उस जहाँ के
बीच चहलकदमी हो रही है:
ये किस ख़ता की सज़ा में हैं दोहरी जंजीरें
गिरफ़्त मौत की है ज़िन्दगी की क़ैद में हूँ
शराब मेरे लबों को तरस रही होगी,
मैं रिन्द तो हूँ मगर तिश्नगी की क़ैद में हूँ
किसी के रुख़ से जो पर्दा उठा दिया मैंने
सज़ा ये पाई कि दीवानगी की क़ैद में हूँ
न जाने कितनी नकाबें उलटता जाता हूँ
जनम जनम से मैं बेचेहरगी की क़ैद में हूँ
गिरफ़्त मौत की है ज़िन्दगी की क़ैद में हूँ
शराब मेरे लबों को तरस रही होगी,
मैं रिन्द तो हूँ मगर तिश्नगी की क़ैद में हूँ
किसी के रुख़ से जो पर्दा उठा दिया मैंने
सज़ा ये पाई कि दीवानगी की क़ैद में हूँ
न जाने कितनी नकाबें उलटता जाता हूँ
जनम जनम से मैं बेचेहरगी की क़ैद में हूँ
अपनी हस्ती को भुला देने, अपने को बेचेहरा
बना देने को ही साधना में सन्त
और फ़क़ीर लगे रहते हैं। जनाब ‘नूर’ लखनवी साहब उस
बेचेहरगी की क़ैद में अपने को जनम-जनम से मानते हैं। इस जनम-जनम की
क़ैफ़ियत भी जान लीजिए :
जन्म जन्म का चक्कर इक अजीब चक्कर है
कश्तियाँ हैं ख़्वाबों की, नींद का समन्दर है।
कश्तियाँ हैं ख़्वाबों की, नींद का समन्दर है।
असल में ‘नूर’ साहब
उर्दू शायरी के उस मुक़ाम पर
पहुँचे हुए शायर हैं जहाँ साहित्य के सारे वाद-छायावाद, रहस्यवाद,
प्रगतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद सब एक जगह इकट्ठे अपनी छटाएँ बिखेरते हैं।
लेकिन सारे वादों से परे उनका आदर्शवाद सोच के किनारों को हर वक्त थपकियाँ
देता रहता है। उनका आदर्शवाद कोरा आदर्शवाद नहीं है, यथार्थ से सीधे
जुड़कर चलता है। इस यथार्थवाद को सँवारने में वे मानवीय मूल्यों के सहारे
के सिवा कोई और सहारा नहीं ढूँढ़ते। मानवीय मूल्यों की गिरावट से वे अन्दर
तक लहूलुहान हो जाते हैं। हो ही नहीं जाते, दिखाई भी देते हैं। याद कीजिए
उनका वह शेर :
तमाम जिस्म ही घायल था घाव ऐसा था
कोई न जान सका रखरखाव ऐसा था
कोई न जान सका रखरखाव ऐसा था
साँचा उनका परम्परागत हो सकता है लेकिन
उसमें ढलनेवाली तस्वीरें आज की
ज़िन्दगी की खरी, सच्ची तस्वीरें हैं। उन सच्ची तस्वीरों में उनके सोच की
बारीकी के रंग हैं जो तल्ख़ से तल्ख़ को नाज़ुक बिम्बों में उतार कर उनका
खुरदरापन निकाल देते हैं। ग़ौर करें—
अपनी पलकों से उसके इशारे उठा
ओर की उँगलियों से शरारे उठा
ओर की उँगलियों से शरारे उठा
वे परम्परा में डूबे हुए शायर हैं मगर उनकी
ग़ज़लों में और नज़्मों में भी
उर्दू शायरी की परम्परागत गुलो-बुलबुल की आशिक़ की चाक गरेबानी आदि का कोई
स्थान नहीं है। बेवफ़ाई इश्क़ की एक अनिवार्य रंगत है लेकिन उसे
‘नूर’ ने अपने अन्दाज़ और मौलिकता से नए बिम्ब प्रदान
किए हैं। ज़िक्र जिस्म का कर रहे हैं लेकिन अन्दाज़ देखिए—
ये जिस्म सबकी आँखों का मरकज़ बना हुआ
बारिश में जैसे ताजमहल भीगता हुआ
बारिश में जैसे ताजमहल भीगता हुआ
और फिर इश्क़ का वह दूसरा पहलू जिसका ज़िक्र
पहले कर चुका हूँ—
मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था
उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है
उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है
इससे अलग जाइए और ज़िन्दगी की ख़ुद्दारी की
थरथराहट देखिए :
उससे अपना ग़म कहकर किस क़दर हूँ
शर्मिन्दा
मैं तो एक क़तरा हूँ और वह समन्दर है
हज़ार ग़म सही दिल में मगर ख़ुशी यह है,
हमारे होंठों पे माँगी हुई हँसी तो नहीं
जबीं को दर पे झुकाना ही बन्दगी तो नहीं
ये देख, मेरी मुहब्बत में कुछ कमी तो नहीं।
मैं तो एक क़तरा हूँ और वह समन्दर है
हज़ार ग़म सही दिल में मगर ख़ुशी यह है,
हमारे होंठों पे माँगी हुई हँसी तो नहीं
जबीं को दर पे झुकाना ही बन्दगी तो नहीं
ये देख, मेरी मुहब्बत में कुछ कमी तो नहीं।
उनकी यह ख़ुद्दारी ख़ुदा को भी
ललकार बैठती है और उसे इस बात का एहसास करा
देना चाहती है कि दहलीज़ पर मत्था टेकना ही इबादत में शुमार न कीजिए
परवरदिगार, मेरी मुहब्बत में कोई कमी नज़र आई हो तो बताइए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book